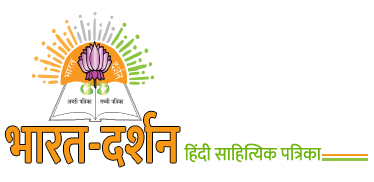मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम 'धनपत राय' था।
...
आलेख
इस श्रेणी के अंतर्गत
जीवन सार | प्रेमचंद की आत्मकथा
मेरा जीवन सपाट, समतल मैदान है, जिसमें कहीं-कहीं गढ़े तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खण्डहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। मेरा जन्म सम्वत् १९६७ में हुआ। पिता डाकखाने में क्लर्क थे, माता मरीज। एक बड़ी बहिन भी थी। उस समय पिताजी शायद २० रुपये पाते थे। ४० रुपये तक पहुँचते-पहुँचते उनकी मृत्यु हो गयी। यों वह बड़े ही विचारशील, जीवन-पथ पर आँखें खोलकर चलने वाले आदमी थे; लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गये और खुद तो गिरे ही थे, उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। पन्द्रह साल की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल ही भर बाद परलोक सिधारे। उस समय मैं नवें दरजे में पढ़ता था। घर में मेरी स्त्री थी, विमाता थी, उनके दो बालक थे, और आमदनी एक पैसे की नहीं। घर में जो कुछ लेई-पूँजी थी, वह पिताजी की छ: महीने की बीमारी और क्रिया-कर्म में खर्च हो चुकी थी। और मुझे अरमान था, वकील बनने का और एम०ए० पास करने का। नौकरी उस जमाने में भी इतनी ही दुष्प्राप्य थी, जितनी अब है। दौड़-धूप करके शायद दस-बारह की कोई जगह पा जाता; पर यहाँ तो आगे पढ़ने की धुन थी-पाँव में लोहे की नहीं अष्टधातु की बेडिय़ाँ थीं और मैं चढऩा चाहता था पहाड़ पर!
...
प्रेमचंद की लघु-कथा रचनाएं
कई वर्ष पूर्व डॉ. कमल किशोर गोयनका ने एक बातचीत के दौरान मुझसे कहा था कि प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य खोजते हुए उन्हें उनकी 25-30 लघुकथाएं भी प्राप्त हुई हैं और वे शीघ्र ही उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित करेंगे । हम, लघुकथा से जुड़े, लोगों के लिए यह बड़ी उत्साहवर्धक सूचना थी । इस बहाने कथा की लघ्वाकारीय प्रस्तुति के बारे में प्रेमचंद की तकनीक को जानने समझने में अवश्य ही मदद मिलती । हालांकि प्रेमचंद को उपन्यास-सम्राट माना जाता है, परन्तु वे कहानी-सम्राट नहीं थे-यह नहीं कहा जा सकता ।
...
प्रेमचंद: कवियों की नज़र में
उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं, बल्कि एक युग-प्रवर्तक थे। उनका विराट व्यक्तित्व और आम आदमी के दुख-दर्द को वाणी देने वाली उनकी लेखनी ने न केवल पाठकों को, बल्कि कवियों को भी गहराई से प्रभावित किया। यही कारण है कि हिंदी-उर्दू के अनेक महत्वपूर्ण कवियों ने प्रेमचंद को अपनी कविताओं और रचनाओं का विषय बनाया।
...
प्रेमचंद की पत्रकारिता | आलेख
पत्रकारिता एक मिशन के रूप में
मुंशी प्रेमचंद को आमतौर पर उनके कथा-साहित्य के लिए जाना जाता है, लेकिन उनका पत्रकार व्यक्तित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए पत्रकारिता केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण का एक सशक्त माध्यम थी। वे मानते थे कि साहित्य "राजनीति के आगे मशाल" है, और यही धारणा उनकी पत्रकारिता में भी झलकती है।
...
प्रेमचंद : घर में
प्रेमचन्द की पत्नी शिवरानी द्वारा लिखी, 'प्रेमचंद : घर में' पुस्तक में शिवरानी ने प्रेमचन्द के बचपन का उल्लेख किया है। यहाँ उसी अंश को प्रकाशित किया जा रहा है।
...
रिस्टवॉच | संस्मरण
एक बार बनारसीदास चतुर्वेदी ने प्रेमचन्द को मज़ाक में पत्र लिखकर शिवरानी (प्रेमचंद की पत्नी) को कलाई घड़ी दिलने की सिफ़ारिश की। चतुर्वेदी ने पत्र में लिखा -
...
प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां | आलेख
लेखक हमेशा यही चाहता है कि उसकी सब रचनाएं सुंदर हों, पर ऐसा होता नहीं। अधिकांश रचनाएं तो यत्न करने पर भी साधारण होकर रह जाती हैं। अच्छे-से-अच्छे लेखकों की रचनाओं में भी थोड़ी सी चीजें अच्छी निकलती हैं। फिर उसमें भी भिन्न-भिन्न रुचि की चीजें होती हैं और पाठक अपनी रुचि की चीज़ों को छांट लेता है और उन्हीं का आदर करता है। हर एक लेखक की हरएक चीज, हरएक आदमी को पसंद आ जाए, ऐसा बहुत कम देखने में आता है।
...
साहित्य का उद्देश्य | अध्यक्षीय भाषण
'प्रगतिशील लेखक संघ', के प्रथम अधिवेशन लखनऊ में 10 अप्रैल, 1936 को सभापति के रूप में प्रेमचंद द्वारा दिया गया भाषण।
...
मैं कहानी कैसे लिखता हूँ | आलेख
मेरे किस्से प्राय: किसी-न-किसी प्रेरणा अथवा अनुभव पर आधारित होते हैं, उसमें मैं नाटक का रंग भरने की कोशिश करता हूँ मगर घटना-मात्र का वर्णन करने के लिए मैं कहानियाँ नहीं लिखता। मैं उसमें किसी दार्शनिक और भावनात्मक सत्य को प्रकट करना चाहता हूँ। जब तक इस प्रकार का कोई आधार नहीं मिलता, मेरी कलम ही नहीं उठती। आधार मिल जाने पर मैं पात्रों का निर्माण करता हूँ। कई बार इतिहास के अध्ययन से भी प्लाट मिल जाते हैं लेकिन कोई घटना कहानी नहीं होती, जब तक कि वह किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को व्यक्त न करे।
...
प्रेमचंद की विचार यात्रा | आलेख
प्रेमचंद ने सन 1936 में अपने लेख ‘महाजनी सभ्यता' में लिखा है कि ‘मनुष्य समाज दो भागों में बँट गया है । बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है, और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का था जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को बस में किए हुए हैं । इन्हें इस बड़े भाग के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं, जरा भी रू -रियायत नहीं। उसका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाए, खून गिराए और चुपचाप इस दुनिया से विदा हो जाए।' इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि प्रेमचंद की मूल सामाजिक चिंताएँ क्या थीं ।
...
प्रेमचन्दजी का स्मारक | माधुरी, दिसंबर 1936
माधुरी (दिसंबर, 1936) के स्थायी स्तम्भ ‘हमारा दृष्टिकोण’ के अंतर्गत प्रेमचंद के बारें प्रकाशित निम्नलिखित सामग्री प्रकाशित हुई--
...
प्रेमचंद की सर्वोत्तम 15 रचनाएं
मुंशी प्रेमचंद को उनके समकालीन पत्रकार बनारसीदास चतुर्वेदी ने 1930 में उनकी प्रिय रचनाओं के बारे में प्रश्न किया, "आपकी सर्वोत्तम पन्द्रह गल्पें कौनसी हैं?"
...
क्या आप जानते हैं?
यहाँ प्रेमचंद के बारे में कुछ जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं। हमें आशा है कि पाठकों को भी यह जानकारी लाभप्रद होगी।
...
प्रेमचन्दजी का स्वर्गवास | माधुरी नवंबर, 1936
8 अक्तूबर, 36 को प्रेमचन्द की मौत हो गई। 8 अक्तूबर, 36 को प्रेमचन्द बहस-मुबाहसे, स्नेह और कटु आलोचना से परे हो गए। यह हिन्दी के सबसे महान् साहित्यिकार का भाग्य है कि तुच्छ और ख़ुदग़रज मुबाहसे से परे होने के लिए 60 साल की उम्र में उसे मरना पड़ा... जिस उम्र में साहित्यिक, क़लमनवीसी से ऊपर उठता है, महात्मा और प्रेरक समझा जाता है और गोर्की के नाम पर शहर और वायुयान बने हैं। प्रेमचन्द को हिन्दी से साधारण समादर न मिल सका। वह अपनी प्रशंसक जनता के इतना निकट रहे कि उनका व्यक्तित्व सदैव साधारण बना रहा। पत्रिकाओं में कहानियाँ छपवाते, सिनेमा से धन पैदा करते, पुस्तकों की बिक्री के लिए साधारण प्रयत्न करते 8 अक्तूबर ’36 को प्रेमचन्द की मौत हो गई।
...
प्रेमचन्दजी के साथ दो दिन | प्रेमचंद से साक्षात्कार
"आप आ रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। अवश्य आइये। आपने न-जाने कितनी बातें करनी हैं।
...
प्रेमचंद : जीवन और साहित्य | आलेख
प्रेमचंद के जीवन के विषय में आप सबने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा। उनके जीवन की मुख्य घटनाओं के उल्लेख की या उनके साहित्य की किसी सूची की यहां आवश्यकता नहीं है। उनके विषय में आज साधारण विधार्थी भी जितना आवश्यक है उतना जानता है, कि वह कब पैदा हुए, कितने दिन गरीबी से किस प्रकार संघर्ष करते रहे, कब दिवंगत हुए, उनकी पैतृक संपदा क्या थी, उनकी शिक्षा किन आपदाओं के बीच हुई, उनका जीवन कितना सीधा-सादा सामान्य तथा अभावों से पूर्ण था। वह किसानों और निम्नतम निम्नमध्य वर्ग की सीमा के प्रतिनिधि थे। आजीवन उन्होंने इसको स्वीकार किया। अपने वर्ग की समस्त असंगतियों, विभीषिकाओं को झेला, उनसे संघर्ष किया और अंत में परास्त भी हुए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि यदि जीवन की सामान्यतम सुविधाएं भी उनको उपलब्ध होतीं तो वह अपना जीवन कम से कम दो दशक तो खींच ले जाते। यह इतना कड़वा सत्य है कि इसे स्वीकार करते समय मैं कांप जाता हूं। पर यह कहता इसलिए हूं कि अब तक उनके अंदर वह मानसिक चैतन्य और जीवनी शक्ति थी, जो उनको जीने पर विवश करती थी। किंतु शरीर ने साथ नहीं दिया। अंत तक वह सांसारिक और छोटी-छोटी चिंताओं से मुक्त नहीं हो सके, जीवन की न्यूनतम सुविधाएं नहीं जुटा सके। पर यह सच अब ऐतिहासिक तथ्य है और आप इसे जानते हैं, जानकर क्लेश पाते हैं। जो बात नहीं जानते वह शायद यह है कि उनकी मानवता किस कोटि की थी। आज वह शब्द इतना हलका हो गया है, कि इसे जितना भी चाहे उछाल सकते हैं पर प्रेमचंद के काल में यह न तो इतना हलका ही था, न इतना प्रचलित। इस समय मानवतावादी होना एक कठिन तपस्या थी। एक बलिदान था, जो तब की परिस्थितियों में और भी कष्टसाध्य था। पर प्रेमचंद की अंतरतम गहराइयों में इस मानवता के अलावा जीने का कोई प्रयोजन, कोई तक नहीं था। वह मानव प्रेम उनके अस्तित्व का एकमात्र सम्बल था। इस तथ्य को लोगों ने इतनी गहराई से नहीं पकड़ा है जितना कि और बातों को। उनका सारा जीवन अपने आदर्शों की स्थापना और पुनर्स्थापना में बीता। उनका व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन समान था। उनके व्यक्तित्व में कहीं किसी प्रकार की विसंगति न थी। मानवता को वह सच्चे हृदय से प्रेम करते थे। इसमें किसी प्रकार का दिखावा न था, उनका मानव प्रेम वह नकाब या मुखौटा न था तो आज की सभ्यता का सबसे बड़ा अस्त्र है और जिसके उपयोग से इस और परलोक की साधना की जाती है। उनकी मानवता वह तात्विक टट्टी न थी, जिसके पीछे से शिकार करना सभी दृष्टियों से निरापद होता है। उनका मानव प्रेम वह नकारात्मक निर्लिप्ति नहीं थी जिसमें मानवता के प्रति एक निर्दय उपेक्षा का भाव ही प्रधान होता है। यही गहनतम सचाई उनके साहित्य के प्रत्येक शब्द में मुखरित है और वही उनके साहित्य की महानता का रहस्य है। उनसे बड़े साहित्यकारों की विश्व-साहित्य में कमी नहीं है। वहां महान विभूतियों का एक अक्षय भंडार है। पर प्रेमचंद यदि वहां पहुचंते हैं तो अपने व्यवहार और दर्शन की एकात्मकता के बल पर ही, क्योंकि साहित्य वह मुकुर है, जिसमें साहित्यकार की सच्ची तस्वीर दिखाई देती है। उस दृष्टि से प्रेमचंद भारतीय साहित्य में अद्वितीय हैं। प्रेमचंद के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी पारदर्शी सच्चाई है, जो उस साहित्य के सृजक के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी थाती थी। उनका व्यक्तित्व ही उनके साहित्य में मुखर हो उठा, मूर्त हो उठा। कहा जाता है कि उनके साहित्य का कला पक्ष निर्बल था। यदि इस कथन में कोई तथ्य है तो यही हो सकता है कि नग्न, कठोर सत्य संभवतः उतना कलापूर्ण नहीं होता, जितना ढका हुआ असत्य। उनके चरित्र इतने प्राणवान्, इतने सशक्त इसीलिए हैं कि वे अपनी सभ्यता में, अपनी संपूर्णता में उद्घाटित हुए हैं। प्रेमचंद ने अपने जीवन के विशाल अनुभव से उनको अनुप्रमाणित किया और उस अनुभव से स्वयं उनका जीवन, उनकी मान्यताएं, उनका आदर्श, उनका जीवन-दर्शन सभी कुछ आलोकित हुआ। यही उनकी महानता, उनकी सर्वप्रियता का रहस्य है। इस तथ्य को, इस सचाई को बार बार दुहराने की आवश्यकता इसीलिए हैं कि इसी में उनके साहित्य के स्रोत हैं। जो साहित्यकार अपनी धरती, अपने आकाश, अपने पेड़, पल्लव, अपने अनुजों के जितना समीप होता है वह उतना ही बड़ा द्रष्टा होता है। उसे वह दृष्टि मिलती है, जो उसके मन प्राण को आलोक प्रदान करती है और वह भविष्य के अदृष्ट को भी वेध सकता है। इस दृष्टि से प्रेमचंद उस देश के इने गिने भविष्य दृष्टाओं में से एक थे।
...
प्रेमचंद और समकालीन सामाजिक विषमता | आलेख
मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हिंदी साहित्य का पुरोधा कहा जाता है, अपने समय की सामाजिक विषमताओं, अन्याय और शोषण के विरुद्ध एक शक्तिशाली आवाज़ थे। उनके कथा साहित्य में ग्रामीण जीवन की पीड़ा, किसानों की दुर्दशा, जातीय भेदभाव, नारी शोषण, सांप्रदायिक वैमनस्य और पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव का जो सजीव चित्रण मिलता है, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक और विचारणीय है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रेमचंद के 'कथानक' आज भी हमारे समकालीन समाज में जीवित हैं, भले ही उनका स्वरूप कुछ बदल गया हो।
...