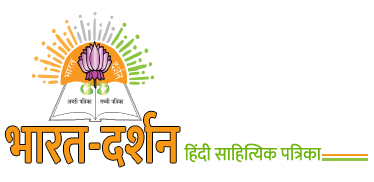मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हिंदी साहित्य का पुरोधा कहा जाता है, अपने समय की सामाजिक विषमताओं, अन्याय और शोषण के विरुद्ध एक शक्तिशाली आवाज़ थे। उनके कथा साहित्य में ग्रामीण जीवन की पीड़ा, किसानों की दुर्दशा, जातीय भेदभाव, नारी शोषण, सांप्रदायिक वैमनस्य और पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव का जो सजीव चित्रण मिलता है, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक और विचारणीय है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रेमचंद के 'कथानक' आज भी हमारे समकालीन समाज में जीवित हैं, भले ही उनका स्वरूप कुछ बदल गया हो।
प्रेमचंद का युग और सामाजिक यथार्थ
प्रेमचंद का लेखन काल 20वीं सदी की शुरुआत का वह दौर था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, सामंती व्यवस्था अपने चरम पर थी, और समाज कई तरह की रूढ़ियों और विषमताओं से ग्रस्त था। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में इसी यथार्थ को ईमानदारी से प्रस्तुत किया।
किसानों की दुर्दशा और शोषण
'गोदान' इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। होरी की त्रासदी भारतीय किसान के शोषण की अमर गाथा है। सूदखोर महाजन, भ्रष्ट पटवारी और निष्ठुर जमींदार किस तरह एक मेहनतकश किसान का रक्त चूसते थे, इसे प्रेमचंद ने मार्मिकता से उकेरा।
जातिवाद और अस्पृश्यता
'ठाकुर का कुआँ', 'सद्गति' जैसी कहानियों में दलितों के प्रति समाज के क्रूर व्यवहार, उनके अमानवीय शोषण और जातीय भेदभाव की पराकाष्ठा को दिखाया गया है।
नारी की स्थिति
प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में नारी जीवन की विडंबनाओं, उनके त्याग, संघर्ष और शोषण को बखूबी चित्रित किया। 'निर्मला' में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की त्रासदी, 'सेवासदन' में वेश्यावृत्ति के कारणों और 'गबन' में नारी की आभूषण प्रियता को सामाजिक बुराई के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।
सांप्रदायिक सौहार्द और वैमनस्य
'मन्दिर' और 'ईदगाह' जैसी कहानियों में प्रेमचंद ने धर्म के नाम पर होने वाले आडंबर और वैमनस्य पर चोट की, वहीं मानवता और सहिष्णुता की गहरी भावना को भी उभारा।
पूंजीवाद और शहरीकरण का प्रभाव
जैसे-जैसे प्रेमचंद का लेखन परिपक्व होता गया, वे शहरी जीवन और बढ़ते पूंजीवाद के प्रभावों को भी अपनी कहानियों में शामिल करने लगे। 'कर्मभूमि' और 'गबन' इसके उदाहरण हैं।
समकालीन सामाजिक विषमता
क्या बदला है?
आज हम 21वीं सदी में हैं। भारत एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश के रूप में उभरा है। शहरीकरण बढ़ा है, सूचना क्रांति आई है और आर्थिक उदारीकरण ने समाज को एक नई दिशा दी है। लेकिन, क्या प्रेमचंद द्वारा उठाई गई सामाजिक विषमताएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं? दुर्भाग्यवश, उनका स्वरूप भले ही बदल गया हो, उनकी मूल आत्मा आज भी जीवित है।
किसानों की बदहाली
'गोदान' का होरी आज भी जीवित है, भले ही वह अब साहूकार के बजाय बैंकों और मौसम की मार से त्रस्त हो। कृषि संकट, कर्ज का बोझ और आत्महत्याएं आज भी भारतीय किसानों की नियति बनी हुई हैं। बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लिए नीतियां बनती हैं, लेकिन छोटे और सीमांत किसान आज भी संघर्षरत हैं।
जातिवाद का अदृश्य स्वरूप
'ठाकुर का कुआँ' भले ही भौतिक रूप से न दिखे, लेकिन जातीय भेदभाव का ज़हर आज भी समाज में गहराई तक फैला हुआ है। गाँवों में आज भी दलितों के प्रति दुर्व्यवहार, सम्मान के नाम पर हत्याएं और उच्च शिक्षा तथा रोज़गार में अप्रत्यक्ष भेदभाव जारी है। शहरी परिवेश में यह सूक्ष्म और अदृश्य हो गया है, लेकिन मौजूद है।
नारी की दोहरी चुनौती
'निर्मला' और 'सेवासदन' की नारियाँ आज शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, लेकिन उन पर सामाजिक और पारिवारिक दबाव अब भी कायम है। दहेज आज भी एक अभिशाप है, भले ही वह 'उपहार' के नाम पर लिया जाए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और पितृसत्तात्मक सोच आज भी नारी की प्रगति में बाधक है। बलात्कार और लैंगिक असमानता के आंकड़े प्रेमचंद के दौर से बहुत अलग नहीं हैं, बस उनके तरीके बदल गए हैं।
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण:
प्रेमचंद ने जिस सांप्रदायिक वैमनस्य की बात की थी, वह आज राजनीतिक लाभ के लिए और भी तीखा और मुखर हो गया है। धार्मिक पहचान पर आधारित नफरत और विभाजनकारी शक्तियां समाज को लगातार बाँट रही हैं। 'मन्दिर' की भावना आज 'घृणा' में बदल गई है, और 'ईदगाह' की भाईचारे वाली सौहार्द कम होती जा रही है।
बढ़ती आर्थिक असमानता:
प्रेमचंद ने पूंजीवाद की आहट महसूस की थी। आज पूंजीवाद अपने विकराल रूप में है। धन का केंद्रीकरण कुछ हाथों में हो गया है, जबकि एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई लगातार चौड़ी हो रही है। 'होरी' जैसे लोग आज भी अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं पाते, जबकि 'रायसाहब' जैसे लोग नए-नए रूपों में समाज पर हावी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया और उपभोक्तावाद ने एक नया वर्गभेद पैदा कर दिया है, जहाँ डिजिटल डिवाइड भी एक बड़ी विषमता है।
भ्रष्टाचार और तंत्र का पतन
प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में सरकारी तंत्र, पुलिस और न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया था। आज भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है। छोटे-मोटे कामों के लिए रिश्वत देना, प्रभावशाली लोगों द्वारा कानूनों का उल्लंघन करना और आम आदमी का न्याय के लिए भटकना, ये सब आज भी हमारे समाज का हिस्सा हैं।
प्रेमचंद की प्रासंगिकता और आज की चुनौती
प्रेमचंद के कथानक इसलिए आज भी जीवित हैं क्योंकि उन्होंने केवल तात्कालिक समस्याओं का चित्रण नहीं किया, बल्कि मानवीय स्वभाव की गहरी समझ और सामाजिक संरचना के मूलभूत दोषों को उजागर किया। उनकी कहानियाँ हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम एक समाज के रूप में कहाँ खड़े हैं और हमने क्या खोया है।
आज की पीढ़ी, जो डिजिटल दुनिया में जी रही है, उसे प्रेमचंद के साहित्य से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यह साहित्य हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, समाज के वास्तविक मुद्दों से परिचित कराता है और हमें एक अधिक संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है।
उनकी रचनाएँ केवल समस्याएँ नहीं दिखातीं, बल्कि मानवीयता, संघर्ष और आशा का संदेश भी देती हैं। 'ईदगाह' का हामिद, 'पूस की रात' का हल्कू, या 'गोदान' की धनिया - ये सभी पात्र अपनी परिस्थितियों से जूझते हैं, लेकिन जीवन जीने की अपनी जिजीविषा नहीं छोड़ते। यह आशावाद ही प्रेमचंद को कालजयी बनाता है।
आज की चुनौती यह है कि हम प्रेमचंद के आईने में अपने समाज को देखें। हमें यह समझना होगा कि तकनीक और आर्थिक प्रगति के बावजूद, यदि हम सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय मूल्यों को स्थापित नहीं कर पाते, तो हम एक खोखले समाज का निर्माण कर रहे होंगे। प्रेमचंद का साहित्य हमें उन 'रेशमी धागों' की याद दिलाता है जो एक समाज को जोड़े रखते हैं, भले ही वे अब कुछ ढीले पड़ गए हों।
प्रेमचंद ने हमें सिखाया कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जगाने और बदलने का एक सशक्त माध्यम है। जब तक हमारे समाज में विषमताएँ, शोषण और अन्याय मौजूद रहेगा, तब तक प्रेमचंद के कथानक जीवित रहेंगे और हमें उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। हमें उनके साहित्य से यह सीखना होगा कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ 'होरी' को न्याय मिले, 'ठाकुर के कुएँ' सबके लिए खुले हों, और 'निर्मला' जैसी लड़कियों को अपनी ज़िंदगी चुनने का अधिकार मिले।
प्रेमचंद का साहित्य एक सतत अनुस्मारक है कि असली प्रगति तब होती है जब समाज का सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी सम्मान और समानता के साथ जीवन जी सके। उनके कथानक आज भी हमारे ज़मीर को झकझोरते हैं और एक बेहतर, न्यायपूर्ण समाज की दिशा में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।
मुंशी प्रेमचंद का साहित्य सिर्फ़ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह हमारे समकालीन समाज का जीवंत दर्पण है। उनकी कहानियों के पात्र और उनकी समस्याएँ आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। उनकी 145वीं जयंती पर, यह आवश्यक है कि हम उनके आदर्शों को न केवल याद करें, बल्कि उन्हें अपने जीवन और समाज में आत्मसात करने का प्रयास करें।
-सुशील शर्मा