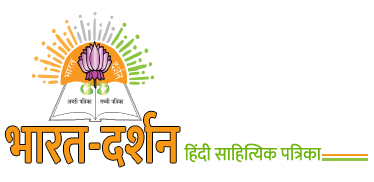8 अक्तूबर, 36 को प्रेमचन्द की मौत हो गई। 8 अक्तूबर, 36 को प्रेमचन्द बहस-मुबाहसे, स्नेह और कटु आलोचना से परे हो गए। यह हिन्दी के सबसे महान् साहित्यिकार का भाग्य है कि तुच्छ और ख़ुदग़रज मुबाहसे से परे होने के लिए 60 साल की उम्र में उसे मरना पड़ा... जिस उम्र में साहित्यिक, क़लमनवीसी से ऊपर उठता है, महात्मा और प्रेरक समझा जाता है और गोर्की के नाम पर शहर और वायुयान बने हैं। प्रेमचन्द को हिन्दी से साधारण समादर न मिल सका। वह अपनी प्रशंसक जनता के इतना निकट रहे कि उनका व्यक्तित्व सदैव साधारण बना रहा। पत्रिकाओं में कहानियाँ छपवाते, सिनेमा से धन पैदा करते, पुस्तकों की बिक्री के लिए साधारण प्रयत्न करते 8 अक्तूबर ’36 को प्रेमचन्द की मौत हो गई।
यदि प्रेमचन्द का एक तुच्छ प्रशंसक आज लिखता है कि 8 अक्तूबर, 36 को हिन्दी-साहित्य की एक शताब्दी पर काल की मुहर लग है। वह एक 'अति प्रेमी' के लांछन से कैसे बचेगा।
प्रेमचन्द हिन्दी की एक शताब्दी थे। भविष्य का साहित्य-इतिहास इस युग से प्रेमचन्द को लेकर बाक़ी इतमीनान से छोड़ देगा।
इसके अनेक कारण हैं। यह नहीं कि उन्होंने 50 ऐसी कहानियाँ पैदा कीं, जो विश्व साहित्य में अपना स्थान बना सकती हैं।
उन्होंने हिन्दी साहित्य में एक नये जीवन का आह्वान किया। नहीं। उन्होंने साहित्य का असली रूप हिन्दी को दिया, उन्होंने मौलिकता सृजन की, उन्होंने मौलिकता को एक द्रुत सजग वेश दिया, उन्होंने जैनेन्द्र पैदा किया।
प्रेमचन्द की प्रतिभा और जीनियस खुद पैदा-करदाँ थी। वह शेली नहीं था, टैगोर नहीं था। शुरुआत में वह एक लिखने का शौकीन था, बीच में एक कठिन संग्राम करता हुआ कलाकार और बाद में एक कैरेक्टर।
वह कैरेक्टर कैसा था?
ऐसा नहीं, जैसा गांधी या टालस्टाय, जो संसार की सहस्र फन विषमता को एक बिंदु पर आकर मिटा देता है, जो मुख्यतः और वस्तुत्तः कवि हो जाता है। उसका कैरेक्टर उसकी अनेकता थी।
ऐसी अनेकता, ऐसी Variety की मिसाल विश्व-साहित्य में भी नहीं है। वह मोपासाँ की morbidity से मी ऊँचा उठ गया।
उसके जीवन में एक स्वर सुनाई देता था कि वह समय के पीछे छुट गया, उसके साथी तो Victorian कलाकार थे और मरने के बाद तो वह विक्टोरियन हो ही गया। पर ऐसा विक्टोरियन, जो पूर्ण सहानुभूति में विश्वास रखता था जो हनन करना भी जानता था, जो प्रकार और आकार में भेद कर सकता था, जो अपनी कला के लिए कच्चा माल लेने बार-बार सीधा जीवन तक जाता था, जो समझता था. जो केवल विश्लेषक नहीं था।
(बी० पी०)
[माधुरी के नवंबर, 1936 के अंक में उपर्युक्त 'प्रेमचन्दजी का स्वर्गवास' प्रकाशित हुआ और इसके लेखक के रूप में (बी० पी०) लिखा हुआ था--बी० पी० यानी भुवनेश्वर प्रसाद।]