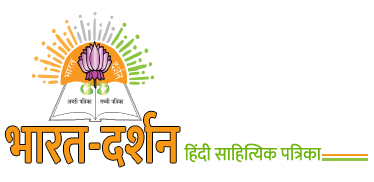उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं, बल्कि एक युग-प्रवर्तक थे। उनका विराट व्यक्तित्व और आम आदमी के दुख-दर्द को वाणी देने वाली उनकी लेखनी ने न केवल पाठकों को, बल्कि कवियों को भी गहराई से प्रभावित किया। यही कारण है कि हिंदी-उर्दू के अनेक महत्वपूर्ण कवियों ने प्रेमचंद को अपनी कविताओं और रचनाओं का विषय बनाया।
प्रेमचंद की सामाजिक चेतना और रहनुमाई
प्रेमचंद ने उस दौर में लिखा जब देश पराधीन था और समाज रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। वे शोषितों और वंचितों की आवाज़ बने। नज़ीर बनारसी प्रेमचंद को इसी रूप में याद करते हैं:
"बनके टूटे दिलों की सदा प्रेमचन्द,
देश से कर गये हैं वफ़ा प्रेमचन्द।
जब कि पूरी जवानी प’ था साम्राज,
उस ज़माने के हैं रहनुमा प्रेमचन्द।"
बाबा नागार्जुन ने प्रेमचंद द्वारा जगाई गई चेतना के चमत्कार को महसूस किया। वे होरी, गोबर और बलचनमा जैसे पात्रों को अब अपना अधिकार लेता देख रहे हैं, जिसकी मशाल प्रेमचंद ने जलाई थी:
"तुम जला गये हो मशाल,
बन गया आज वह ज्योति-स्तम्भ।
कोने-कोने में बढ़ता ही जाता है किरनों का पसार,
लो, देखो अपना चमत्कार!"
प्रेमचंद का भाषा-शिल्प और पात्र-सृष्टि
प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू को एक साथ लाकर 'हिन्दुस्तानी' भाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। गौरीशंकर मिश्र 'द्विजेंद्र' उनके इसी योगदान को नमन करते हैं:
"हिंदी-उर्दू बहन-बहन को गले मिलाया,
आपस के चिर बैर भाव को मार भगाया।"
उनकी कहानियों के पात्र इतने जीवंत हैं कि वे पाठक के मन में बस जाते हैं। गुलज़ार इसी अनुभव को बड़ी ख़ूबसूरती से बयाँ करते हैं कि प्रेमचंद को पढ़ना आसान नहीं, क्योंकि उनके पात्र आपका पीछा नहीं छोड़ते:
"प्रेमचंद की सोहबत तो अच्छी लगती है,
लेकिन उनकी सोहबत में तकलीफ़ बहुत है..."
प्रेमचंद को कवियों की श्रद्धांजलि
अनेक कवियों ने उन्हें सीधे-सीधे श्रद्धांजलि अर्पित की है। केदारनाथ अग्रवाल उनके जन्मदिवस पर पुष्प चढ़ाने का आह्वान करते हैं:
"आज हर्ष की बीन बजाओ,
प्रेमचंद का दिवस मनाओ;
अश्रु नहीं, शत् पुष्प चढ़ाओ,
अमर यशस्वी कथाकार की
कृतियों पर सर्वस्व लुटाओ।"
प्रगतिशील कवि त्रिलोचन शास्त्री ने सीधे तौर पर प्रेमचंद पर कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन उनकी प्रसिद्ध कविता 'उस जनपद का कवि हूँ' की आत्मा प्रेमचंद की दुनिया से गहराई से जुड़ी है। जब त्रिलोचन कहते हैं:
"उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा-दूखा है...
प्रेमचंद ने जिनका
साहित्य रचा, जीवन जिनकी कहानी है।"
प्रेमचंद का प्रभाव केवल उन कविताओं तक सीमित नहीं है जो सीधे तौर पर उन्हें श्रद्धांजलि देती हैं। उनकी चेतना और उनका वैचारिक संघर्ष कई कवियों की रचनाओं में गूँजता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं गांधीवादी कवि भवानीप्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता 'जाहिल के बाने'।
यद्यपि यह कविता सीधे प्रेमचंद को संबोधित नहीं है, पर इसका नायक 'मैं' हूबहू प्रेमचंद का किसान-नायक 'होरी' है, और इसका खलनायक 'आप' वही 'महाजनी सभ्यता' का शोषक वर्ग है जिसके खिलाफ प्रेमचंद ने आजीवन लिखा। यह कविता 'सभ्य' और 'जाहिल' के बीच के पाखंड को उजागर करती है, जो प्रेमचंद के साहित्य का केंद्रीय स्वर है। कविता के ये अंश देखिए:
"मैं असभ्य हूँ क्योंकि खुले नंगे पाँवों चलता हूँ
मैं असभ्य हूँ क्योंकि धूल की गोदी में पलता हूँ
मैं असभ्य हूँ क्योंकि चीरकर धरती धान उगाता हूँ
मैं असभ्य हूँ क्योंकि ढोल पर बहुत ज़ोर से गाता हूँआप सभ्य हैं क्योंकि धान से भरी आपकी कोठी
आप सभ्य हैं क्योंकि ज़ोर से पढ़ पाते हैं पोथी
आप सभ्य हैं क्योंकि आपके कपड़े स्वयं बने हैं
आप सभ्य हैं क्योंकि जबड़े ख़ून सने हैंमैं उतारना नहीं चाहता जाहिल अपने बाने
धोती-कुरता बहुत ज़ोर से लिपटाए हूँ याने!"
यह कविता प्रेमचंद के कथा-संसार का मानो काव्यात्मक सार हो, जहाँ शोषित अपनी गरीबी और तथाकथित 'जाहिलियत' के बावजूद अपने स्वाभिमान और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दृढ़ है।
डॉ. दिनेश चमोला 'शैलेश' ने तो 'भावर्षि प्रेमचंद तुम्हें प्रणाम' कविता में उनके पूरे जीवन-संघर्ष और साहित्यिक यात्रा को ही समेट दिया है:
"धनपत राय श्रीवास्तव तुम थे,
तुम्हीं अजायब सुत नवाब राय भी।
उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद भी तुम,
थे साहित्य सिद्ध, जीवन अभिप्राय।"
बदलते दौर में प्रेमचंद की प्रासंगिकता
साहित्य और समाज के बदलते मूल्यों पर भी कवियों ने प्रेमचंद को याद किया। हास्य कवि शैल चतुर्वेदी व्यंग्य के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे साहित्यिक बाज़ारवाद कालजयी रचनाओं को हाशिये पर धकेल रहा है:
"किताब वाले से पूछा: 'प्रेमचंद का गोदान है?'
तो बोला: 'गोदान!
यह नाम तो पहली बार सुना है श्रीमान...'"
इसी तरह, अदम गोंडवी उन छद्म बुद्धिजीवियों पर प्रहार करते हैं जो प्रेमचंद की सामाजिक चेतना को ख़ारिज कर सतही लेखन को बढ़ावा देते हैं:
"प्रेमचन्द की रचनाओं को एक सिरे से खारिज़ करके,
ये 'ओशो' के अनुयायी हैं, कामसूत्र पर भाष लिखेंगे।"
अंततः, प्रेमचंद की कमी आज भी उतनी ही महसूस की जाती है। हरियाणा के राजकवि और ' हिन्दी रुबाई सम्राट' उदयभानु हंस का दर्द आज के साहित्यिक सूनेपन को दर्शाता है:
"कौन अब सुनाएगा, दर्द हमको माटी का,
प्रेमचंद गूंगा है, हुआ लापता निराला है।"
इन कविताओं से स्पष्ट है कि प्रेमचंद केवल एक कथाकार नहीं, बल्कि एक साहित्यिक और सामाजिक कसौटी हैं, जिसके पैमाने पर हर पीढ़ी के कवि साहित्य और समाज को परखते रहे हैं। उनकी जलाई मशाल आज भी राह दिखा रही है और इसीलिए, प्रेमचंद कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। वे सचमुच अमर हैं।
-रोहित कुमार हैप्पी