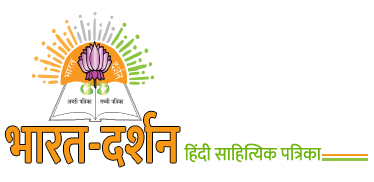ट्रक को आते देख कर उसकी ख़ुशी का ठिकाना न रहा। वह इतनी ख़ुश थी कि अपनी ख़ुशी को व्यक्त करने के लिए उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। बचपन से ही उसका दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने का सपना अब साकार होने जा रहा था। इस दिन का इंतज़ार वह बचपन से करती आई थी।
जब कभी उसे शादी-ब्याह में दिल्ली जाने का अवसर मिलता तो वह बहुत ख़ुश होती। वहाँ उसे अपनी चचेरी-मौसेरी बहनों को देख कर ख़ुशी और जलन दोनों का आभास होता। उनकी बातों, कपड़ों, फ़ैशन और आत्मविश्वास को देख कर उसे अपने बौनेपन का एहसास होने लगता। सोचती, वह सब कहाँ की कहाँ पहुँच गईं हैं और मैं हाउस वाइफ़ की हाउस वाइफ़ ही रह गयी हूँ। अगर दिल्ली में होती तो क्या की क्या बन जाती। हो सकता है राजनीति में ही चली जाती। अब तक सोशल वर्कर या फिर एम.एल.ए. तो ज़रूर बन गयी होती। वैसे भी दिल्ली में रहने वालों की तो बातें ही न्यारी-व्यारी होती हैं। क्या फड़ाके की अंग्रेज़ी बोलते हैं। कितने मॉडर्न लगते हैं। ख़ुश थी कि आज के बाद, उसकी बचपन की गुड़िया के घर का दरवाज़ा खुलने वाला था, जिसमें कई वर्षों से उसने अपने सपने संजो कर रखे थे।
ट्रक भी आ गया था। ट्रक में सामान ढोने से पहले शिखा ने ड्राइवर और उसके दो साथियों को सामान की लिस्ट की कॉपी पकड़ा दी और उन्हें समझाया कि लाल लिखाई वाले डब्बे रसोई में, नीले बैठक में इत्यादि। सब डब्बों पर लिखा है कहाँ क्या रखना है। उसने भाग-भाग कर घर के सभी कमरों का निरीक्षण किया, कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। कुल डब्बे गिने, अपनी लिस्ट देखी। शिखा ने सब डब्बों को कलर-कोडेड कर ही दिया था। तय यह हुआ कि उसके पति समीर सामान के साथ ट्रक में सफ़र करेंगे। शिखा बच्चों के साथ अपनी कार में। लुधियाना से दिल्ली का सफ़र लम्बा था, कार में उसने रास्ते के लिये पानी और कुछ खाने का सामान रख लिया था। ट्रक भरने के पश्चात्, यही तय हुआ कि कार और ट्रक दोनों साथ-साथ जाएँगे। फ़ोन तो सबके पास थे ही।
रास्ते भर शिखा के मस्तिष्क में अनेकों प्रश्न उठने लगे, कि इतने बड़े शहर में वह अकेली कैसे निर्वाह कर पायेगी। रिश्तेदार तो दूर रहते। आस-पड़ोस में तो कोई परिचित भी नहीं है। मेड कहाँ से ढूँढ़ेगी? सब कुछ नए ढंग से सीखना पड़ेगा। लोगों के मिज़ाज कैसे होंगे? अकड़ू तो नहीं होंगे? वहाँ का वातावरण कैसा होगा? सुना है दिल्ली में बड़े-बड़े मॉल हैं जहाँ केवल डिज़ाइनर चीज़ें ही मिलती हैं। शिखा को ख़ुशी के साथ-साथ उत्सुकता भी होने लगी। फिर ख़ुद पर ही हँसने लगी... पगली कहीं की... बड़बड़ाने लगी... क्यूँ इतना घबरा रही है, जो होगा देखा जाएगा। दिल्ली ही तो जा रहे हैं, चाँद पर थोड़े ही। दिल्ली पहुँचते-पहुँचते दो बज गए। दोपहर का खाना तो ढाबे में खा लिया था। जैसे ही ट्रक घर के सामने लगा, चारों ओर पड़ोसी बड़ी उत्सुकता से अपनी-अपनी खिड़कियों से झाँकने लगे। यह तो स्वाभाविक था ही। ट्रक वालों को कमरों में सलीक़े से सामान टिकाते-टिकाते दो घंटे लग गए थे, हालाँकि समीर ने अपने दफ़्तर से दो लड़के मदद के लिये बुला लिये थे। जैसे ही सब चले गए, समीर ने कहा, “शिखा, अपना बैग निकालो, भूख लगी है।” शिखा ने इधर-उधर देखा, बैग कहीं नहीं था। उसे एहसास हुआ कि शायद बैग ढाबे में ही रह गया है।
अभी सोच ही रहे थे क्या करें? दरवाज़ा खुला था... फिर भी शिष्टाचार के नाते किसी ने घर की घंटी बजाई। समीर और शिखा हैरान थे। कौन हो सकता है? हम तो किसी को जानते भी नहीं यहाँ। शिखा दरवाज़े तक गयी, उसे देखते ही वह हैरान सी उसे देखती रही। दरवाज़े पर एक बूटे क़द का आदमी खड़ा था। उसके शरीर का गठन आम लोगों से थोड़ा हट कर था। उम्र शायद चालीस की होगी। कहना मुश्किल था। वह हाथ जोड़ते हुए बोला, “नमस्ते, मैं निर्मल हूँ, आपके सामने वाले घर में अपनी माँ और मेरी बेटी आस्था के साथ रहता हूँ। सोचा आप लोग सफ़र के बाद थके होंगे।” वह शिखा को एक बैग पकड़ाते हुए बोला, “मैं आपके लिये थोड़ा चाय-नाश्ता लाया हूँ। कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े कृपया बेझिझक फ़ोन कर देना। अपना फ़ोन नम्बर मैंने लिख कर बैग में रख दिया है।” इतना कह कर वह चला गया, किन्तु अपनी उदारता की छाप छोड़ गया। निर्मल के उदार भाव से दोनों इतने भावुक हो गए कि धन्यवाद जैसा शब्द उनके अधरों पर ही ठहर गया। सबने चाय-नाश्ता किया। चाय के अतिरिक्त बैग में दूध, डबलरोटी, अंडे, चीनी, चायपत्ती, मक्खन, बिस्कुट इत्यादि थे। हाँ, एक लिस्ट भी थी जिसमें वहाँ की स्थानीय दुकानों के फ़ोन नम्बर भी थे। निर्मल तो चला गया, अपना एक हिस्सा उनके पास छोड़ गया था। दोनों यही सोचते रहे किसी के बाहरी आवरण को देख कर उसके चरित्र का आँकलन नहीं करना चाहिए। बेशक उसका कद छोटा था, चाल में मतवालापन था, बोलने का अन्दाज़ भी निराला था, पर था वह शख़्स इंसानियत से भरपूर, भगवान का बनाया हमारे-तुम्हारे जैसा इंसान। आहिस्ता-आहिस्ता वह अपनी सादगी से शिखा के परिवार का एक हिस्सा बन गया। उसकी एक बहन भी थी।
पड़ोसियों की ताक-झाँक के साथ-साथ उनकी उत्सुकता बढ़ती गयी। उस दिन मार्केट में पड़ोसन ने शिखा को देखते ही अपना रास्ता बदलकर कहा, “नमस्ते जी, मैं मिसेज़ कपूर, आपके साथ वाले घर में रहती हूँ।” बस, हो गयी शुरू... बातों-बातों में उसने पूछ लिया... “क्या आप निर्मल को पहले से जानती हो? आपके यहाँ आता-जाता है? उससे बच कर रहना। कोई भी उसे मुँह नहीं लगाता। थोड़ा दिमाग़ का ढीला है। चुग़लियाँ करता है। जब छोटा था तो बच्चे उससे खेलते थे। जैसे-जैसे बड़ा होता गया, सभी उससे कन्नी काटने लगे। पता नहीं लगता कि लड़का है या लड़की? किसी के भी तो लक्षण नहीं हैं उसमें। भगवान ही जाने क्या है? हाँ, अपनी माँ का लाड़ला है।” मिसेज़ कपूर एक ही साँस में बहुत कुछ बता गयीं। मैंने कहा, “मिसेज़ कपूर, आपको ग़लतफ़हमी हुई है। निर्मल तो बिलकुल निर्मल है... अपने नाम की तरह।” शिखा ने घड़ी देखी, अपना पीछा छुड़ाते हुए बोली, “माफ़ करना मिसेज़ कपूर, बच्चे आने वाले हैं, अब मैं चलती हूँ।” घर पहुँचते ही परिवार में लीन हो गयी। हैरान थी, लोग कैसे बेबुनियादी बातें करने लगते हैं। मिसेज़ कपूर की बातें उसके दिमाग़ में घूमती रहीं... सोचने लगी, तभी तो निर्मल की आँखों से एक बेबसी सी झाँकती रहती है। लगता है, समाज के थपेड़ों ने उसके एहसास ख़त्म कर दिए हों। हैरान थी, कितनी चुस्ती से क्षण भर में वह निर्मल का रेफ़्रेन्स सर्टिफ़िकेट दे गयीं।
अब शिखा दिल्ली की चहल-पहल और उसके जीवंत वातावरण का आनंद लेने लगी थी। किंतु आस-पड़ोस के लोगों के मिज़ाज और उनके तौर-तरीक़े शिखा की समझ के बाहर थे। उनका अभिमानपूर्वक व्यवहार, चुगलख़ोरी का स्वभाव, अपने को ऊँचा औरों को नीचा जतलाने की कोशिशों से उसे बहुत नफ़रत थी। धीरे-धीरे शिखा ने ख़ुद को महानगर के तौर-तरीक़ों के अनुकूल बना लिया था। अब तो उसकी कई लोगों से पहचान हो गयी थी, उनके यहाँ आना-जाना तो आरंभ नहीं हुआ था। यहाँ-वहाँ सैर करते टकराव हो जाता। कभी-कभार नमस्ते के साथ मुस्कुराहटों का लेन-देन भी हो जाता।
एक दिन अचानक घंटी बजी, छः नम्बर वाली कुसुम मेहरा अपनी बेटी के विवाह का निमंत्रण देने आयी थीं। बोलीं, “ज़रूर आना, आस-पास के पड़ोसियों से मेल-मिलाप भी हो जायेगा।” कुसुम जल्दी में थीं... बैठी तो नहीं, किन्तु जाते-जाते ठुनका मारते हुए बोलीं, “शिखा, तुम छोटे-छोटे बच्चों वाली हो। उस छक्के से दूर ही रहा करो। आत्मसम्मान और आत्मस्वाभिमान जैसी चीज़ तो उसके कभी क़रीब से भी नहीं गुज़री। लोग उसे फटकारते रहते हैं, उसे कोई फ़र्क़ ही नहीं पड़ता।” इतना कह कर कुसुम चली गयी। 'छक्का' शब्द ने उसे सोच में डाल दिया। यह शब्द उसके लिए नया था।
शादी का दिन भी आ गया। दूर-दूर से बनावटी मुस्कानों का आदान-प्रदान हुआ। लड़की वाले थे... इसलिये खाना खाने की बारी देर से आयी। जहाँ मिसेज़ कपूर खड़ी थीं, शिखاा भी वहीं जाकर खड़ी हो गयी। इतने में कुसुम मेहरा ने आकर सबसे शिखा का परिचय करवाया। शिखा पर प्रश्नों की भरमार लग गयी... कहाँ से आयी हो? पति क्या करते हैं? बच्चे कितने हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं? वग़ैरह-वग़ैरह। थोड़ी बहुत खाने की आलोचना हुई। इतने में शिखा की नज़र निर्मल और उसकी माँ पर पड़ी, उसने संकेत से उन्हें वहीं बुला लिया। उन्हें उसी ओर आते देखते ही मानो सबको साँप सूँघ गया। उनकी भौंहें चढ़ गईं... माथे की लकीरें गहरी हो गईं। सभी शिखा की ओर विस्मय से देखने लगीं... मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो।
उनके वहाँ से जाते ही सब निर्मल पर उछल पड़ीं, यकायक निर्मल के प्रति सघन नकारात्मक बातों का अंबार लग गया। ऊषा सेठी नकारात्मक लहजे से बोलीं, “बहन, हम तो इसे पैदा होने से जानते हैं। सब कुछ ठीक ही था। सबके साथ स्कूल जाता था, हाँ कॉलेज भी गया था, हाँ अपने पापा के निधन के पश्चात् कॉलेज में देर तक टिक नहीं पाया। उसकी माँ ने भी ज़ोर नहीं डाला। उसमें अजीब से बदलाव आते गये। क़द तो बूटा है ही, अपने पापा की तरह गोल-मोल भी है और बुद्धि भैंस की।” कुछ ही मिनटों में उसका इतिहास दोहरा डाला।
“लोग उसे दुत्कारते..., उस पर हँसते..., मज़ाक़ उड़ाते..., उसे कोई फ़र्क़ ही नहीं पड़ता।” कुसुम ने चाट मसाला लगाते हुए कहा। “नौकरी तो करता है, कोई मामूली सी... हाँ, माँ के साथ चिपका रहता है। माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटाता है। सब औरतों वाले काम करता है, स्वेटर बुनता है, रोटी बनाता है, कपड़े धोता है। मेड नहीं रखी।” उनकी बेतुकी बातों से शिखा का सर चकराने लगा, उसका मन किया, इसी वक़्त यहाँ से भाग जाए। सोच ही रही थी कि मिसेज़ कपूर वहाँ आ पहुँचीं।
मिसेज़ कपूर कहाँ चुप रहने वाली थीं, झटपट बोलीं, मानो ख़बरी चैनल को इंटरव्यू दे रही हों, “पता है, निर्मल की दो पत्नियाँ तो इसे जल्दी ही छोड़ भाग गयीं थीं। तीसरा रिश्ता निर्मल की बहन संगीता का पति संजय ले कर आया था। रिश्ते में वह उसकी बहन लगती थी, ऐसा उसने बताया था। पता नहीं लोग ऐसे लोगों को अपनी लड़कियाँ दे कैसे देते हैं, इस छक्के को? एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन। भला टिकती भी क्यूँ, इस आधे-अधूरे के साथ। संगीता के निधन के पश्चात् तीसरी बीवी आशा भी निर्मल को छोड़ कर चली गयी। आशा से निर्मल की एक बेटी हुई, आस्था। सभी ख़ुश थे, अब तो बड़ी हो गयी है, फ़ाइनल ईयर में है। पर हाँ, आस्था को निर्मल ने बहुत लाड़-प्यार से पाला है। बढ़िया ब्रांडेड कपड़े लाता था उसके लिये। आस्था की हर माँग को पूरा करता है। उसकी माँ और आस्था दोनों निर्मल की जान हैं। निर्मल का हर पल आस्था पर केंद्रित था।”
कितनी मलिन सोच है समाज की, शिखा की सोच से बाहर था। क्यूँ निर्मल का नाम सुनते ही लोगों की भौंहों पर बल पड़ जाते हैं? माथे की लकीरें गहरी हो जाती हैं? स्वर में कसैलापन झलकने लगता है? देता क्या है समाज उसे... उपेक्षा, तिरस्कार... फटकार और लानतों-मलानतों का पुरस्कार? उस दिन निर्मल ठीक ही तो कह रहा था, “दीदी, पत्थर की दीवार गिराना आसान है, किंतु रवैयों की दीवार गिराना बहुत मुश्किल है। तंग आ गया हूँ, कोई निर्मल कौर कहता है और कोई निर्मल सिंह, कोई छक्का और कोई फ़िफ़्टी-फ़िफ़्टी। जब देखो नए नाम का अविष्कार कर लेते हैं। अब दुःख भी दुःख नहीं लगते, बहुत गहरे हो गये हैं, यूँ कहो आदत पड़ गयी है।” इतना कह कर वह चला गया।
इस बात को हुए चार-पाँच दिन बीत चुके थे, निर्मल की कोई ख़बर नहीं थी। निर्मल की बातें उसे उदास कर देती थीं। उसे सोचने पर विवश कर देती थीं... “कि क्या वह इसी हृदयहीन समाज की सदस्य है? जहाँ इंसान के साथ जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता है।” शिखा ने ठान लिया कि वह निर्मल के सामाजिक संत्रास को कम तो नहीं कर सकती, पर उन पर मित्रता की मरहम तो लगा सकती है। उसने दिल्ली में कुछ बनने के सपने को स्थगित कर दिया। निर्मल में आत्मविश्वास पैदा करने का प्रण ले लिया।
एक सप्ताह से निर्मल दिखायी नहीं दिया। शिखा चिंतित थी। निर्मल की माँ से पूछा, उन्होंने बताया, “कुछ दिन के लिये अंबाला गया है। भाई के घर काम हो रहा है, वह छुट्टी ले नहीं सकता। मज़दूरों पर नज़र रखने के लिये... उसे कोई घर का आदमी चाहिए था। सप्ताहांत तक आ जाएगा।”
“ठीक है, मैं चलती हूँ। आपको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े कृपया बता देना। निर्मल नहीं, हम तो हैं यहाँ।” शिखा ने उनकी पीठ थपथपाते हुए उनका माथा चूमा। ख़ुशी से उनके चेहरे पर तीन इंच की मुस्कुराहट फैल गयी। लगता था, शायद निर्मल के कारण उन्हें भी आउट-कास्ट कर दिया हो, कोई ढंग से बात ही नहीं करता। शिखा असमंजस में थी। इतनी क्रूरता! इंसान से! कोई नहीं जानता, किसी के साथ कभी भी, कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है।
शिखा बरामदे में खड़ी थी। उसने देखा, निर्मल ठुमक-ठुमक कर हाथ में कुछ लिये उसकी तरफ़ ही चला आ रहा था। वह गोल-मोल तो था ही, चाल में भी मस्ती थी। माथे के टीके से लगता था कि मन्दिर से आ रहा है। अंदर आते ही हाथ में एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोला, “यह लो, मैंने आज गजरेला बनाया है... आज आस्था का जन्मदिन है। शाम को उसे वहीं ले जाऊँगा, जहाँ वह चाहेगी।” वह कभी ख़ाली हाथ नहीं आता, सदा कुछ न कुछ बना कर लाता था। यह उसकी आदत है। दिल का बहुत अमीर है। “अच्छा, अब चलता हूँ।” “अरे, थोड़ी देर बैठो तो सही,” शिखा ने कहा। जैसे ही वह रॉकिंग-चेयर पर बैठा, शिखा समझ गयी कि आज कुछ कहना चाहता है। वह जानती थी कि जब कोई भी बात उसे कुरेदती है... तो वह रॉकिंग-चेयर पर बैठ कर झूलने लगता है। बोलने लगा, “शिखा दीदी, लोगों को मैं अच्छा क्यूँ नहीं लगता? इतनी नफ़रत क्यूँ करते हैं मुझसे? क्यूँ दुत्कारते रहते हैं मुझे? कोई निर्मल देवी कहता है, कोई निर्मल रानी, तो कोई निर्मल सिंह।”
“यहाँ तक कि रिश्तेदार भी बहुत निरादर करते हैं। मामा जी का काम करवाने गया था। बेवजह गालियाँ खा कर वापस आया हूँ। मामी सदा टोकती रहती थीं, ‘अपने मामाजी की शराब कम पिया कर, बहुत महंगी है, इम्पोर्टेड है।’ कभी इज़्ज़त, प्यार से नहीं बुलाया किसी ने। संजय ने तो बहुत फ़ायदा उठाया मेरा। हमेशा हुक्म ही चलाता रहता था, यह ले आ, वो ले आ। और ख़ुद मेरी बीवी के साथ घुटने से घुटना लगाकर बैठा रहता था। मैंने माँ को कभी नहीं बताया, नहीं तो लफड़ा हो जाता, बहनोई था मेरा। वैसे भी माँ मेरे कारण किस-किस से झगड़ा करती। रहना तो समाज में ही है।” “निर्मल, बातें तो बड़ी समझदारी की करते हो, रिश्तों की अहमियत का भी एहसास है तुम्हें, पर कभी-कभी झल्ला जाते हो,” शिखा ने अर्थपूर्ण मुस्कान से कहा। आज उसका मन बहुत भरा हुआ था, आज वह मुस्कुराया नहीं। वह आँखों में घिर आई बदली को पी गया। बड़बड़ाता रहा, “क्यूँ... क्यूँ इतना अभिशप्त है जीवन मेरा? कई बार अपने को मुक्त करना चाहा, सोचा सब कुछ छोड़ कर भाग जाऊँ। हर बार माँ की तस्वीर सामने आ जाती।” कुछ देर तेज़ी से झूल-झूल कर चुपचाप बिन कुछ कहे चला गया।
कुछ दिनों से निर्मल यहाँ-वहाँ डोलता दिखाई नहीं दिया। शिखा ने बाहर खेलते बच्चों से पूछा। किसी ने भी उसे नहीं देखा था। हार कर वह निर्मल के घर पहुँची, मोबाइल फोन तो उन दिनों थे नहीं। निर्मल की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। शिखा ने चारों ओर नज़रें घुमायीं। निर्मल दिखायी नहीं दिया। उसकी मम्मी ने बताया, “कुछ दिन से वह बहुत उदास है। अपने कमरे में है। प्रकोप में बैठा है... अपनी झूलने वाली रॉकिंग कुर्सी पर। कारण भी नहीं जानता। भूल जाता है क्यूँ दुखी है।” इतना कहते ही उनकी आँखें भर आयीं, बोलीं, “क्या बताऊँ बेटा, कई बार तो हम दोनों के दरम्यान झील सी गहरी ख़ामोशी ठहर जाती है।” “हुआ क्या है, खुल कर बताएँ। चिंता न करें, बात कहीं नहीं जायेगी,” शिखा ने आश्वासन देते हुए कहा।
“क्या बताऊँ, बड़ी लंबी गाथा है। निर्मल के साथ ही आरम्भ हुई थी। नौ महीने तो कोख में रखा। फिर प्यार और आँचल की छत्रछाया से ढका उसे। थोड़ा अलग सा दिखने के कारण सबकी दुत्कार का निशाना बना। उसके पापा के जाने के बाद, काँटों की सेज पर चल कर हर ज़िम्मेवारी को निभाने की कोशिश की है। जी भर के प्यार दिया। देती भी क्यूँ न, माँ हूँ न? भाग्य तो नहीं बदल सकती थी। किंतु उसके ललाट पर लिखी विधि की अदृश्य लिपि को मिटा तो नहीं सकती थी... उसकी स्याही तो हल्की कर सकती थी... जो कभी किसी ने नहीं देखी थी। वह लिपि कठोर आघातों की कठिन यात्रा थी। उम्र भर उसके चेहरे पर कभी पीड़ा की रेखाएँ खिंचतीं... कभी अंतर्वेदना की और कभी अपराध-बोध भावना की। अब देखो न, सात दिन से निर्मल ने ख़ुद को कमरे में बंद किया हुआ है। कह रहा था... ‘माँ, अब तो बच्चे मेरा नाम ले-ले कर आस्था को भी छेड़ने लगे हैं। उसका मज़ाक़ उड़ाते हैं।’ निर्मल का प्रत्येक क्षण आस्था के भविष्य के जाल बुनने में लगा रहता है। आस्था उसकी जान है। वह कहता है, ‘आस्था के लिये जीवन समर्पित कर दूँगा। यही मेरा लक्ष्य है।’ लोगों ने मेरे जिगर के टुकड़े की खिल्ली उड़ा कर उसको भी हीन भावना से ग्रस्त कर दिया है... जिसमें वह आज तक क़ैद है।”
“निर्मल ने आस्था के लिये बड़े सपने देखे हैं। एक आस्था का होना ही उसे जीने के लिए बाध्य करता है। आस्था उसके जीने का सबब है। वह प्रत्येक क्षण बेटी के भविष्य के बारे में जाल बुनता रहता है। बड़ी हो रही है, सोचती हूँ, कल को उसकी शादी होगी, तो कैसे जी पायेगा मेरा लाल। वह घंटों दर्पण में अपना चेहरा देख कर सोचता है... मैं ऐसा क्यूँ हूँ। उस वक़्त मैं... अपना चेहरा आइने में उसके साथ जोड़ कर खड़ी हो जाती हूँ और कहती हूँ... देख बेटा, हम दोनों के चेहरे तो एक जैसे हैं। वही नाक, वही आँखें, वही मुँह, वही रंग... तू अलग कैसे हो सकता है। अक्सर रातों को उसकी सिसकियाँ सुनायी देती हैं। ऐसा लगता है उसको भीतर से कुछ खाये जा रहा हो, किंतु पूछने से घबराती हूँ, माँ जो हूँ न, मजबूर हूँ,” निर्मल की माँ सुबकती रहीं... शिखा पास बैठी उनके जीवन की विसंगतियों और विडंबनाओं के बारे में सोचती रही।
भारी मन से शिखा अपने घर पहुँची। वह जो देख और सुन कर आयी थी... उसकी सोच से परे था। सोचती रही, इतनी विकृत मानसिकता क्यूँ है हमारे समाज की? कितनी सरलता से कोई भी किसी के आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ा देता है। कितना संवेदनहीन हो गया है हमारा समाज? पाँच-छः दिन बीत गये। शिखा निर्मल की सहायता के लिए विकल्प ढूँढने लगी। उसे लगा एक मनोवैज्ञानिक ही निर्मल के मन में बैठी कुंठाओं, चिन्ताओं को बाहर लाने में सफल हो सकता है। हो सकता है कि वह अनजान व्यक्ति से खुल कर बात कर ले। यह भी मुमकिन है कि माँ और बेटा दोनों मानें ही न, क्यूँकि हमारे समाज में मनोवैज्ञानिक से मिलना भी कोई कलंक से कम नहीं। बड़ी दुविधा में थी वह। चार-पाँच दिन बीत चुके थे, निर्मल की कोई ख़बर नहीं मिली।
सुहानी शाम थी। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। शिखा अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसने देखा, निर्मल सामने से चुपचाप मुँह लटकाए चला आ रहा था। अंदर घुसते न दुआ न सलाम। वह सीधा रॉकिंग-चेयर पर बैठ कर झूलने लगा और रोने लगा। रोते-रोते उसकी हिचकी बंध गयी। सिसकियाँ भरता रहा। शांत होने पर शिखा ने उससे बड़े प्यार से पूछा... “बात क्या है?” “कुछ नहीं, मैं अभी तक जान क्यूँ नहीं पाया कि... कि लोग मुझसे इतनी नफ़रत क्यूँ करते हैं? मुझ पर हँसते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। गालियाँ देते हैं। भद्दे-भद्दे नामों से बुलाते हैं। अल्फ़ाज़ों के कंकर फेंकते रहते हैं। कई बार सोचता हूँ... कितनी मजबूरी होगी मेरी माँ की ममता की कि वह सदा मेरे सामने लोहे की दीवार बन कर खड़ी रही। बहुत अच्छी है मेरी माँ। और एक मैं हूँ, उस पर भार बना बैठा हूँ। कई बार सोचता हूँ इससे अच्छा तो जानवर जाति में जन्म ले लेता। फिर सोचता हूँ क्यूँ? यह भेदभाव तो मनुष्य ने बनाए हैं। पेड़ों को ही देख लो, सभी में फल थोड़े ही लगता है। किसी में बीज भी नहीं होता। दीदी, थक गया हूँ... पत्थर की दीवार गिराना आसान है, किंतु रवैयों की दीवार गिराना बहुत मुश्किल है। साँस लेना तो ज़रूरी है... पर जीना मजबूरी।” कुछ देर वातावरण में मौन पसरा रहा। बाहर जाते-जाते निर्मल कुछ क्षण भावशून्य सा खड़ा रहा, फिर बोला, “मुझमें है ही क्या? मेरा तो शरीर भी किसी काम का नहीं...” कहते-कहते उसकी आँखों से एक बूँद लुढ़की और गाल पे अटक गयी। शिखा ने उसके अनकहे को सुना और महसूस किया। वो तो चला गया। जो कुछ सुना, यक़ीन से बाहर था। यह उसका भयानक इतिहास था। निर्मल उम्र भर अपने अधूरेपन को कुरेदता रहा, यही उस आधे-अधूरे की चकनाचूर करने वाली हक़ीक़त थी। शिखा उसकी मनोस्थिति पर बहुत चिंतित थी। शिखा ने मनोवैज्ञानिक तक पहुँचने का प्रयास किया। वह दो सप्ताह की छुट्टी पर था।
दो दिन बीत चुके थे, शाम को किसी ने ज़ोर-ज़ोर से शिखा का दरवाज़ा पीटना शुरू किया। उसने खोला, एक बच्चा हाँफते-हाँफते बोला, “आंटी... आंटी... आपको निर्मल की मम्मी बुला रही हैं, जल्दी... प्लीज़ बहुत जल्दी।” सुनते ही वह धक से रह गयी। उसकी छठी इंद्री कुछ कह रही थी। उसने जल्दी से चप्पल पहनी और भागी। वहाँ निर्मल की मम्मी सिसकियाँ भर रही थीं। शिखा ने पूछा, “निर्मल कहाँ है?” उन्होंने बंद दरवाज़े की ओर संकेत दिया। वह सिसकते-सिसकते बोलीं, “सब मेरा क़सूर है। मुझे यह काम बरसों पहले ही कर देना चाहिए था। मुझे आस्था को बता देना चाहिए था। सब कुछ जानते हुए भी मैंने अपने बेटे की ख़ुशी के वास्ते आँखें मींच ली थीं। मैं सब कुछ जानती थी कि घर में क्या चल रहा है। संजय वहाँ क्यूँ आता है। निर्मल को क्यूँ बाहर भेजता है। जब आशा पेट से हुई.. मैं जान-बूझ कर अनजान बनी रही। मेरा स्वार्थ आड़े आ गया। मैंने निर्मल के भ्रम को भ्रम ही रहने दिया। तुम्हीं बताओ, बेटे की ख़ुशी को कैसे क़ुर्बान कर सकती थी। उम्र भर झूठ के साथ जीती रही। ख़ुश थी कि अब निर्मल पर कोई अंगुली नहीं उठायेगा, कोई उसे छक्का... फ़िफ़्टी-फ़िफ़्टी और दरमियाना नहीं कहेगा। मैं अपने बेटे की शारीरिक विकृति को जानती थी। सब जानते हुए भी अनजान बनी रही। मुझे पता था, अगर किसी को पता लग गया तो मैं बेटे को खो नहीं पाऊँगी। कैसे बलि चढ़ा देती बेटे की। उम्र भर झूठ के साथ जीती रही।”
“शिखा बेटा, आप कोशिश करें, शायद आपकी बात मान ले।”
“निर्मल, दरवाज़ा खोल प्लीज़। जब तक बताएगा नहीं, तो किसी को कैसे पता चलेगा? तुम्हारे मरने से क्या सब उलझनों का हल निकल आएगा? तेरे बिना क्या ज़िंदा रह सकेगी तेरी माँ? दरवाज़ा खोल, मेरे भाई, बैठ कर कोई हल निकालते हैं।” दरवाज़े में चाबी नहीं थी, शिखा ने चाबी के छेद से देखा, निर्मल अपनी रॉकिंग-चेयर पर झूल रहा था। वह समझ गयी कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। वह टस से मस नहीं हुआ। निर्मल की मम्मी हाथ जोड़ कर बोलीं, “बेटा, माफ़ कर दे। तेरी गुनहगार हूँ।” वह उसके पैर छूने को थी कि उसने उठ के माँ को गले लगा लिया। दोनों एक-दूसरे से लिपट कर ख़ूब रोये। माँ उसके बालों को सहलाती-सहलाती उसकी मनपसंद लोरी गुनगुनाने लगी और वह शांत हो गया। उसे पानी पिलाया और बोलीं, “बेटा, अपने जिगरी दोस्त को नहीं बताएगा?” वह ज़ोर से अपनी माँ से लिपट गया। माँ ने उसे आराम से उसकी रॉकिंग-चेयर पर बैठा दिया। आँखें बंद किये वह झूलता-झूलता बोलता गया।
“माँ, मैंने बार-बार अपने अभिशप्त जीवन से मुक्त होना चाहा। कभी सोचता बेटी ही हो जाता, अधूरा बेटा भी किस काम का। कितनी बार घर छोड़ना चाहा, सम्बंध तोड़ने चाहे। माँ के प्यार की बेड़ियाँ पाँव रोक लेतीं। मुझे ही सब छोड़ कर चले जाते हैं। माँ, अब आस्था भी छोड़ कर चली गयी है। चिट्ठी छोड़ के गयी है। चिट्ठी में लिखा है, ‘पापा निर्मल... मैं सच जान गयी हूँ। आपको मुझे यह सच बहुत पहले बता देना चाहिए था। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मुझे आधे-अधूरे पापा की नहीं, पूरे मम्मी-पापा की ज़रूरत है। मैं अपनी मम्मी-पापा के पास जा रही हूँ। जाते हुए दुःख हो रहा है, मुझे मम्मी भी चाहिए। सॉरी... प्लीज़ लेने मत आना।’ आपकी बेटी, आस्था।”
निर्मल की माँ मुँह में पल्ला ठूँसे, रोती-रोती हाथ जोड़ते हुए बोलीं, “माफ़ करना बेटा, मुझे उसी वक़्त रोक लगा देनी चाहिए थी। मैंने सब कुछ जानते हुए भी अपने बेटे की ख़ुशी के लिये आँखें मींच लीं। संजय का आना मुझे खलता था। हम दोनों ने एक-दूसरे के भ्रम को भ्रम ही रहने दिया। तुम्हीं बताओ, बेटे की ख़ुशी को कैसे क़ुर्बान कर सकती थी।”
“मत रो मेरी माँ, मैं भी जानता था कि तेरी ख़ुशी भी इसी काँच की तरह चकनाचूर करने वाली हक़ीक़त में ही है। माँ हो या बाप हो, बच्चों के लिये प्यार तो एक जैसा ही होता है। मैं अपने भीतर बैठे शख़्स को तसल्ली देता रहा।”
वह आँखें बंद किये रॉकिंग-चेयर पर बैठा तेज़ रफ़्तार में झूलता रहा।
शिखा ने दोनों के कहे-अनकहे को सुना और महसूस किया। वक़्त वहीं थम गया।
-अरुणा सब्बरवाल
ई-मेल: arun.sabharwal45@gmail.com