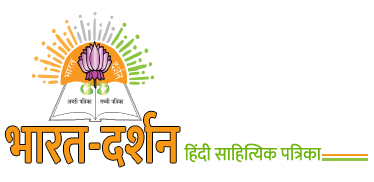डॉ मदनलाल ‘मधु' जी से सुनीता पाहुजा की बातचीत।
(10 अप्रैल 2014)
डॉ मदनलाल ‘मधु' का नाम केवल हिंदी जगत ही नहीं अपितु समग्र भारत और रूस में जाना है। आप प्रख्यात कवि और नाटककार होने के साथ-साथ संपादक और अनुवादक भी रहे हैं। रूस में इतने लम्बे समय से रह रहे सबसे पहले भारतीय हैं। वर्ष 1991 में भारत में पद्मश्री से, 1999 में पुस्कीन सम्मान और 2001 में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मैत्रयीपदक (Friendship Order) से नवाज़ा जाना और भारत और रूस के लोगों से समान रूप से मिली लोकप्रियता उनके द्वारा किए गए कार्य की महत्ता के प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी के माध्यम से डॉ मधु जी और उनकी पत्नी श्रीमती तान्या जी से एक मुलाकात का सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश।
आपका जन्म और स्नातक तक की शिक्षा फिरोज़पुर, पंजाब में हुई और एम.ए. आपने लाहौर से किया। उसके बाद...आपने पढ़ाना शुरु किया?
लाहौर से एम.ए. करने के बाद मैंने शिमला में और जी.एन.एम कॉलेज, अम्बाला कैंट में पढ़ाया, आर.एस.डी कॉलेज, फिरोज़पुर, मेरा जन्मशहर, जो आजकल बॉर्डर पर है, जहाँ से मैंने ग्रेडुएशन की थी ऑनर्स के साथ, 1-2 साल वहाँ भी पढ़ाया, कुल मिलाकर लगभग 10 साल तक पढ़ाया।
रूस जाने का सबब कैसे बना?
हमारे दोनों देशों के जब संबंध बढ़ने लगे थे, वर्ष 1955 में, और उस समय पं. जवाहरलाल नेहरू पहली बार मॉस्को आए थे, साथ में युवा इंदिरा भी थीं। मॉस्को और दूसरे कई शहरों में भी बड़े पैमाने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। और इसी साल रूस के नेता ख्रुश्चेव (Khrushchev) और बुल्गॉनिन (Bulganin) भी भारत यात्रा पर आए। तब दोनों देशों के संबंध बनने लगे थे। यह वो ज़माना था जब शीत युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान तो पश्चिम के साथ चला गया और फौजी ब्लॉक का सदस्य बन गया था पर भारत की नीति तो तट्स्थ रहने की थी, इस तटस्थता ने एक बहुत महत्त्वपूर्ण आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का रूप ले लिया था, जिसमें दुनिया के लगभग सौ से अधिक देश शामिल हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और युगोस्लाविया के टीटो, ये तीन बड़े नेता इसमें शामिल थे और पंडित जी का बहुत महत्व था। सोवियत संघ चाहता था कि उन्हें मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर लाने का, उन्हें हमारी ज़रूरत थी एक तटस्थ देश के रूप में, और हमें ज़रूरत थी उनकी क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना था और अमरीका और पश्चिमी देश भारत का साथ नहीं दे रहे थे। तो पं. नेहरू ने सोवियत संघ की ओर हाथ बढ़ाया और उन्होंने भी हमें सहायता देने का वायदा किया तो इस तरह परस्पर संबंध बढ़े। कश्मीर की समस्या के संदर्भ में उस समय रूस ने कहा था कि हम हिमालय के उस पार बैठे हैं आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम मदद करेंगे। उस समय भारत में कोई उद्योग, इस्पात आदि के कारखाने तो थे नहीं और भारत को विकास की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा कि वे इसमें जहाँ तक हो सकेगा हमारी मदद करेंगे और उस समय सोवियत संघ के साथ मिलकर भारत ने भिलाई का कारखाना और अन्य कई कारखाने, कोई सौ से अधिक उद्यम लगाए। दोनों देशों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं और तभी 1955 में यह समझौता किया गया कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक क्षेत्र में भी संबंध बढ़ने चाहिए। तभी यह भी तय हुआ कि भारतीय भाषाओं के साहित्य का रूसी भाषा में और सोवियत संघ की अन्य भाषाओं में और इसी तरह उनके साहित्य का हमारी भाषाओं में अनुवाद और संपादन किया जाए ताकि लोगों को दोनों देशों के बीच जो सांस्कृतिक पुल है उसका पता लग सके। तब भारत के विदेश मंत्रालय से इस संबंध में एक सर्कुलर आया। मैं उस समय अम्बाला कैंट में पढ़ा रहा था और वहाँ के प्रिंसिपल मुझसे अपार स्नेह करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि में वह फार्म ज़रूर भरूँ। उनके आग्रह को मैं ठुकरा न सका। छह महीने बाद अचानक विदेश मंत्रालय से पत्र आया जिसमें मुझे साक्षात्कार के लिए दिल्ली बुलाया गया था। जब मैं दिल्ली आया तो उस शाम वहाँ मेरी मुलाकात भीष्म साहनी से हुई, उन्हें भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। वे मेरे अच्छे दोस्त थे, हमने अम्बाला कैंट कॉलेज में एकसाथ पढ़ाया भी था और लेखक होने के नाते भी हम बहुत नज़दीक थे विचारों की दृष्टि से, वो कहानीकार थे और मैं एक उभरता हुआ युवा कवि था। रेडियो से भी मेरा संबंध था। 10 साल पढ़ाने के साथ-साथ मैंने 3 साल जालंधर रेडियो स्टेशन पर हिंदी परामर्शदाता और लेखक के रूप में नाट्क और रूपक लिखे। दिन में मैं वहाँ काम करता था और शाम को कक्षाएँ भी लेता था। 3 साल का वहाँ का मेरा अच्छा अनुभव था।
साक्षात्कार के लिए जब हमें बुलाया तो वहाँ बोर्ड में विदेश मंत्रालय के सचिव और अन्य सदस्यों के अलावा संयोगवश हिंदी विशेषज्ञ के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी भी थे। 1951 में जब मेरा कविता संग्रह छपा था ‘उन्माद' तब बच्चन जी का मेरे पास पत्र आया था कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं। उन्हें मेरा कविता-संग्रह बहुत पसंद आया था लेकिन उसके बाद वे केम्ब्रिज चले गए थे पी.एच.डी. करने के लिए तो मुलाकात नहीं हो पाई। 1954 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन वालों ने मुझे एक कवि सम्मेलन के लिए बुलाया था, वहाँ से लौटते समय उन्होंने मुझे इलाहाबाद अपने घर पर बुलाया और मैंने पूरा एक दिन उनके साथ बिताया। वे मुझे इलाहबाद रेडियो स्टेशन ले गए, वहाँ उन्होंने मुझे सुमित्रानंदन पंत जी से मिलवाया, भारत भूषण भी वहाँ काम कर रहे थे और अन्य लेखकों और कवियों से भी मिलवाया। वहीं से मेरा बच्चन जी से परिचय हुआ और फिर पत्र-व्यवहार भी होने लगा था। वे मुझसे और मेरे काम से भली-भांति परिचित थे।
जब हम साक्षात्कार के लिए गए तो वहाँ कोई 30-40 उम्मीदवार थे। कई लोगों के बाद जब भीष्म साहनी का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बाहर आकर मुझे बताया कि अंदर तो बच्चन जी भी बैठे हैं। मैंने जब पूछा कि इंटरव्यू कैसा हुआ तो उन्होंने बताया कि ठीक रहा, लगभग 20-25 मिनट तक उनसे कुछ सवाल पूछे। जब मैं अंदर गया तो बच्चन जी ने काफी आत्मीयता से मुझे बुलाया। कमेटी के सदस्यों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे और मेरे काव्य-संग्रह और मेरे तमाम लेख वगैरह देखे।
इंटरव्यू के बाद मैं अम्बाला वापस आकर पढ़ाने लग गया। कोई दो महीने के बाद सोवियत एम्बेसी से पत्र आया कि भारत के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में अनुवादक-संपादक के रूप में काम करने के लिए आपके नाम की सिफारिश की है। हम आपसे मिलना चाहेंगे, आप दिल्ली में हमारे दूतावास में आइए। मैंने दूतावास जाकर उनसे भेंट की और उन्होंने मुझे बताया कि सब कुछ तय हो गया है, आप बताइए कि आप कब मॉस्को जा सकते हैं। मैंने कहा कि मैं बी.ए. और एम.ए. के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, इस वर्ष (1957) सत्र समाप्त होने पर, मार्च के अंत तक, मैं जा सकता हूँ । इस बीच उन्होंने सब व्यवस्था कर दी और 28 मार्च 1957 को मैं मॉस्को पहुँच गया। तब से वहाँ मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 3 साल का पहला अनुबंध था, पर 3 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि आपका काम हमें बहुत अच्छा लगता है आप कुछ समय और रुक जाएँ, और इस तरह 3 साल बढ़ते-बढ़ते तीस साल हो गए, तीस साल फिर चालीस साल और अब तो सत्तावन साल हो गए हैं, (मुस्कराते हुए) मेरा जीवन ही बीत गया मॉस्को में।
रूसी भाषा आपने वहीं जाकर सीखी ? यह विचार मन में कब और कैसे आया ?
हाँ, रूसी वहीं जाकर सीखी। दरअसल हमारे अनुबंध में तो यही था कि हम लोग अंग्रेज़ी के माध्यम से काम करेंगे। यानि रूसी साहित्य का अनुवाद जो अंग्रेज़ी में किया जा चुका था, उसका अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद करेंगे। लेकिन जब पहली ही पुस्तक का मैंने अनुवाद किया तो मुझे अनुभव हुआ कि अंग्रेज़ी के माध्यम से तो बात बनती नहीं। हमारे प्रकाशन-गृह में एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वो यह कि वहाँ कंट्रोल-एडिटर्स थे, यानि जाँच-संपादक। ये ऐसे रूसी लोग थे जिन्होंने संस्था के माध्यम से अच्छी हिंदी सीखी हुई थी और वे हमारे किए हुए अनुवाद की तुलना रूसी टेक्स्ट से करते थे और जहाँ कोई गलती रह जाती थी या कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता था तो वे बताते थे कि नहीं यहाँ पुश्किन (मूल लेखक) ने तो ये कहा है या तॉल्स्तॉय (मूल लेखक) ने तो ऐसा कहा है, तो अंग्रेज़ी से हिंदी करते समय जो गड़बड़ होती थी वो हमें बताते थे। अंग्रेज़ अपने ढंग से अनुवाद कर देते थे और अंग्रेज़ी चूँकि हमारी मातृभाषा नहीं है तो उनके बहुत सारे स्लैंग्स और लोकल एक्स्प्रैशन हमारी समझ में नहीं आते थे इसलिए ग़लतियाँ होती थीं तो ये जो जाँच-संपादक थे, रूसी, यही उनका काम था। मेरी पत्नी भी यही काम करती थीं, वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो हमारे देश में नहीं है, और मैं कहता हूँ कि होनी चाहिए कि तुलना की जाए मूल पाठ की और उसके अनुवाद की। तब मैंने अनुभव किया कि रूसी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है, तब इनसे (पत्नी से) तो परिचय नहीं था, मैंने ख़ुद अपने यत्न से ही, बहुत मेहनत करके रूसी सीखी और दो साल के बाद तो मैं सीधे रूसी भाषा से ही अनुवाद करने लगा और उसके बाद तो मैं आगे चलता ही गया।
आपकी पत्नी, तान्या जी ने हिन्दी आपके लिए सीखी ?
नहीं, नहीं इन्होंने तो हिंदी बकायदा इंस्टीट्यूट में पढ़ी थी और ये कंट्रोल एडिटर का काम करती थीं (रूसी और हिंदी अनुवाद की तुलना करने का काम)।
(तान्या जी से पूछा) आपको भारत कैसा लगता है ?
वे बोलीं कि बहुत अच्छा लगता है । ‘मधु' जी ने कहा कि ये तो भारत की दीवानी हैं। हम हर साल भारत आते हैं, 2-3 महीने के लिए, कभी मैं नहीं भी आना चाहता हूँ तो ये ज़िद करती हैं कि नहीं चलिए, चलिए।
(तान्या जी बहुत ही अच्छी और स्पष्ट हिंदी बोलती हैं, वे काफी देर तक रूस और भारत के मौसम के बारे में बात करती रहीं)
सोवियत संघ का विघटन आपने देखा, उसका आपके काम पर क्या प्रभाव पड़ा?
1991 के अंत में सोवियत संघ टूटा। उसके बाद से ही हमारे प्रकाशन-गृह बंद हो गए। प्रगति प्रकाशन जिसमें हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया था बंद हो गया, रादुगा प्रकाशन (जिसका मतलब था इंद्रधनुष) यह बंद हो गया, ‘सोवियत नारी' पत्रिका जो हम वहाँ से भेजते थे, इसका मैं साहित्यिक संपादक रहा, इसकी यहाँ भारत में बहुत भारी माँग थी, इतनी कि हम हर महीने इसकी 3 लाख प्रतियाँ भारत भेजते थे। यह बंद हो गई।
1957 से 1991 तक, लगभग 40 वर्ष तक, जो काम वहाँ हुआ उसमें मैंने 100 पुस्तकों का अनुवाद किया जिनमें से 50% बच्चों की पुस्तकें हैं, रूसी बाल साहित्य, रूसी लोक कथाएँ, और उसके अलावा बहुत बड़ा जो काम हुआ, जिसे एक तरह से साहित्यिक काम कहेंगे - उनके महाकवि पुश्किन की कविताएं, उसका बहुत बड़ा संग्रह, दूसरे कवियों की रचनाएं, जैसे मायोवस्की, चेखव इत्यादि, तॉल्स्तॉय के उपन्यास ‘युद्ध और शांति', ‘आना करेनिना', उनकी कहानियाँ, दस्तायवस्की की कहानियाँ, उनके उपन्यास, तुर्गनेव के उपन्यास, चेखव-गोर्की के नाटक, कहानियाँ, तमाम रूसी क्लासिक साहित्य इसमें शामिल था, लगभग 50 किताबें मैंने कीं। वहाँ बहुत काम हो रहा था अनुवाद का, वे लगभग 40 भाषाओं में अनुवाद कर रहे थे, जिनमें अंग्रेज़ी, फ्रैंच, स्पैनिश, जर्मन आदि भाषाएँ थीं। हमें जो दिया जाता था वो अंग्रेज़ी में किया गया होता था, पर जैसे मैंने बताया कि उस तरह अनुवाद करने में वो बात नहीं बनती है, होना यह चाहिए कि अनुवाद मूल पाठ (रूसी) से ही किया जाता। इसी को महसूस करते हुए मैंने रूसी भाषा सीखी और फिर सीधे रूसी से हिंदी अनुवाद करना शुरू किया। कुछ पुस्तकों का संपादन भी किया।
1991 में हुए सोवियत संघ के इस विघटन से वहाँ की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुआ, उसका आपके साहित्यिक सृजन पर क्या प्रभाव पड़ा?
हुआ यह कि उसके बाद मैं पत्रकारिता ज़्यादा करने लगा। ‘नंदन' पत्रिका उस समय निकाल रहे थे कन्हयैलाल नंदन जी, उन्होंने मुझसे अनुरोध किया, नवभारत टाइम्स वालों ने मुझसे कहा तो मैंने उनके लिए और 'संडे मेल साप्ताहिक' और अंग्रज़ी के ट्रिब्यून के लिए लिखना शुरू कर दिया एक संवादाता/समाचार लेखक के रूप में। इस तरह पत्रकारिता और उसके साथ-साथ मौलिक साहित्यिक लेखन ज़्यादा शुरू हो गया क्योंकि अनुवाद कार्य के साथ मौलिक सृजन के लिए समय नहीं मिला करता था। जब मौलिक लेखन बढ़ाना शुरू किया तभी एक पूरा संग्रह ‘गीत-अगीत' निकला जिसमें 80 कविताएँ थीं। यहीं दिल्ली में मेधा बुक्स ने प्रकाशित किया। फिर एक हिंदी-रूसी शब्दकोश बनाया इनके साथ मिलकर (पत्नी की इशारा करते हुए), वह भी बहुत लोकप्रिय हुआ। फिर मैंने अपने संस्मरण लिखने शुरू किए जो दो भागों में छपे, 'यादों के धुँधले उजले चेहरे'। इन दोनों भागों में मेरे जीवन की पूरी कहानी है, बचपन से लेकर, लाहौर की ज़िंदगी, उससे पहले की ज़िंदगी, लाहौर में कैसे तमाम लोगों से मिलना हुआ-- फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, उर्दू के....... जालंधरी, उदयशंकर भट्ट, हरिशंकरप्रेमी, साहिर लुधियानवी - ये तमाम लेखक थे, लाहौर में, उन दिनों में। इन लोगों के साथ अच्छे संबंध बने मेरे और दूसरा भाग मॉस्को में बिताए मेरे जीवन के 57 सालों के बारे में है। उसमें तमाम कहानी है वहाँ के जीवन की, किस तरह का वहाँ का हमारा जीवन था, कैसा हमने अनुभव किया, क्या-क्या कठिनाइयाँ शुरू में आईं, कैसे-कैसे कष्ट हमने झेले । फिर इसमें भारत के 40 जाने-माने लेखक जो मॉस्को आए उनकी कहानी है - सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, यशपाल, कमलेश्वर, मोहन राकेश, डॉ नामवर सिंह, उर्दू के कैफ़ी आज़मी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, इस्मत चुक्ताई - इन सबसे मेरा बहुत ही निकट संबंध रहा, इन सब की कहानी आई है दूसरे भाग में। इनके अलावा जो नेता वहाँ आए, इंदिरा गाँधी कई बार आईं, कितनी बार मिलना हुआ उनसे, ख्रुश्चेव से कितना मिलना हुआ, ब्रेज़्नेव से कितना मिलना हुआ इन सब अनुभवों का ज़िक्र है उसमें।
एक हमने वहाँ सांस्कृतिक संस्था बनाई थी भीष्म साहनी जी के साथ मिलकर - हिंदुस्तानी संवाद। भीष्म साहनी जी तो वहाँ 7 साल रहकर लौट आए थे, चूँकि मैं वहाँ रह गया था तो मैंने ही वह संस्था सम्भाली, लगभग 30 साल तक मैं उसका अध्यक्ष रहा और अब उसका संरक्षक (पैट्रन) हूँ। उस संस्था के मंच पर इन लोगों को आमंत्रित करते रहते थे। इसी कारण नेहरू जी से भी वहाँ मिलना हुआ, शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपयी जी से - संस्था का अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम कार्यक्रम आयोजित करता और इन्हें आमंत्रित करता तो इनसे मिलना होता था, बड़ी-बड़ी बाते होतीं थीं - सब संस्मरण हैं इसमें। वहाँ जो हमारे राजदूत थे, उन सबसे भी अच्छे संबंध थे मेरे, अभी तक भी हैं। उसके अंतिम अध्याय में मैंने दिया है कि क्यों सोवियत संघ टूटा, क्या कारण थे, क्या परिस्थितियाँ थीं और एक तरह से अपना पूरा निष्कर्ष इस एक अध्याय में लिख दिया। पर मुख्य रूप से दूसरा भाग पूरा साहित्यिक और सांस्कृतिक है, मेरे जीवन के व्यक्तिगत अनुभव उसमें आए हैं।
इतने महत्वपूर्ण और जाने-माने लोगों से आपका मिलना जुलना हुआ!
हाँ, मैं अपने आपको बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि इतने बड़े-बड़े लोगों से मेरा इतना निकट का संबंध रहा, घंटों इनके साथ बातें करना - बच्चन जी के साथ, कमलेश्वर के साथ, शिव मंगल सिंह ‘सुमन' जी के साथ, मोहन राकेश और मैं तो लाहौर में एकसाथ पढ़े, इतने लोगों के संपर्क में आना - बहुत ही विरले ऐसा होता है - यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा ।
आपको भारत में पद्मश्री और रूस में ऑर्डर ऑफ फ्रैंडशिप मैडल से सम्मानित किया गया!
ऑर्डर ऑफ फ्रैंडशिप जिसे हिंदी में मत्रैयी पदक कहते हैं, यह रूस का सबसे ऊँचा सम्मान है। 2002 में जब पुतिन राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले उनके हाथों यह सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत बड़ा समारोह हमारे दूतावास में आयोजित किया गया था। लगभग 100-150 लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया था। तमाम रूसी मंत्री, विदेश मंत्री वगैरह वहाँ मौजूद थे। मुझे अपने जीवन में पूरा संतोष है, जो कुछ मेरे जीवन में हो पाया उससे ज़्यादा आदमी और क्या सोच सकता है।
आप न केवल रूस में रह रहे हैं बल्कि सेवा भी कर रहे हैं और रूस में इतने लम्बे समय से रह रहे सबसे पहले भारतीय हैं। जिस समय दोनों देश निकट आ रहे थे आपने उनकी सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक घनिष्ठता को और बढ़ाया और एक सेतु का काम किया।
हाँ मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी किताब ‘यादों के धुँधले उजले चेहरे' का जब विमोचन किया गया, दिल्ली में रूसी दूतावास में, तो मुख्य अतिथि एलेक्ज़ेंडर कदाकिन थे, डॉ नामवर सिंह भी वक्ता थे, कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने इस किताब पर चर्चा की। बाद में एलेक्ज़ेंडर ने इस कार्यक्रम की रिपोर्ट मॉस्को भेजी तो उसमें लिखा कि ये क्ल्चरल ब्रिज-बिल्डर हैं - यानि साहित्यिक-सांस्कृतिक सेतु निर्माता।
आप जब रूस गए तो आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा?
सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की ही थी। हमें रूसी नहीं आती थी और वहाँ अंग्रेज़ी कम लोग जानते थे। जब बाज़ार में जाते थे तो अक्सर चीज़ों के नाम जानने पर भी उस चीज़ की कोई खास किस्म की ज़रूरत होने पर उसे समझाना मुश्किल हो जाता था। जैसे टमाटर के लिए शब्द तो मालूम था, पर चटनी बनाने वाला विशेष टमाटर चाहिए यह समझाना बेहद कठिन हो जाता था। इसीलिए मैंने एक पुस्तक बनाई, रूस आने वाले भारतीयों के लिए 'रूसी-हिंदी बातचीत' जिसमें रोज़मर्रा में काम आने वाले कुछ वाक्य थे जिनमें हिंदी वाक्यों के सामने रूसी भाषा का वाक्य हिंदी में लिप्यांतरित करके दिया होता था जिससे वे उसे देखकर बोल लें। इसी दृष्टि से हिंदी-रूसी शब्दकोश भी बनाया। रूसी विद्यार्थी जो हिंदी सीखते हैं उनके लिए यह बहुत उपयोगी है। और शुरू के सालों में कई कठिनाइयाँ आईं, ठण्ड का मौसम, चीज़ों की उन दिनों में बहुत कमी थी, खासकर उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत कमी थी क्योंकि उनका ज़्यादा ध्यान तो रहता था युद्ध-सामग्री बनाने में, बड़े-बड़े जहाज़ बनाना, रॉकेट बनाना जो युद्ध में काम आ सकें, दूर तक मार कर सकें। तो उपभोक्ता वस्तुओं की अवहेलना होती रही। ज़्यादातर वस्तुएँ वे आयात करते थे।
(मधु जी ने तान्या जी से अपनी कुछ पुस्तकें लाकर हमें दिखाने के लिए कहा । अन्ना करेनीना, यादों के धुँधले उजले चेहरे, प्रेमचंद और गोर्की, पुश्किन का उनके द्वारा किया गया तमाम अनुवाद। और फिर जैसे पुराने वक्त को याद करते हुए मानों वहीं पहुँच गए......बताने लगे...2008 पुस्तक मेले में रूस मेहमान देश था। तब पुश्किन की यह किताब विशेष रूप से छापी गई, आर्ट पेपर पर थी और एक प्रति पर 30-35 डॉलर का खर्च आया और उन्होंने इसकी 500 प्रतियाँ छपवा कर यहाँ भारत में भेंट कीं। इसमें जो चित्र हैं वो भी स्वयं पुश्किन के बनाए हुए हैं।)
आपके पसंदीदा रूसी साहित्यकार कौन हैं?
सबसे पहले तो पुश्किन हैं फिर तॉल्स्तॉय, गोर्की और चेख़व - ये वो लेखक हैं जो मुझे सबसे अच्छे लगे ।
और भारत के?
अगर पुराने ज़माने की बात की जाए तो क्या सूरदास, क्या तुलसीदास, क्या मीरा - ये सब तो मन को बहुत ही छूने वाले रहे हैं विशेष रूप से भक्तिकाल के कवि मुझे बहुत ही पसंद हैं और आधुनिक काल के साहित्यकारों में पंत जी, निराला जी, बच्चन जी की बहुत बड़ी देन रही है, खासकर बच्चन जी मेरे प्रिय कवि भी रहे और उनसे मेरे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। इनके अलावा अज्ञेय जी भी अच्छे थे, कमलेश्वर जी की कहानियाँ भी बहुत अच्छी थीं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हम भी अनुवाद के क्षेत्र से जुड़े हैं, हालाँकि हमारा वास्ता कार्यलयी अनुवाद से रहता है, फिर भी आपसे अनुरोध करेंगे कि कुछ टिप्स दें जिन्हें हम मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकें।
कुछ लोग सोचते हैं कि अनुवाद का काम रुटीन काम है, पर ऐसा है नहीं। वास्तव में अनुवाद का काम सृजनात्मक काम है। कभी-कभी तो यह मौलिक लेखन से भी मुश्किल होता है क्योंकि किसी दूसरे के विचारों को लेकर अपनी भाषा में ऐसे ढंग से पेश करना कि ऐसा लगे कि वह मौलिक रचना है, यह बहुत मुश्किल काम है और इसमें सबसे कठिन काम है ललित साहित्य के अनुवाद का। जहाँ तक विज्ञान का, प्रौद्योगिकी का संबंध है, वहाँ तो इतना ही करना है कि आप तकनीकी शब्दावली तैयार कर लेते हैं। पर उसमें भी यह है कि दोंनो भाषाओं का और दोंनो विषयों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर आप अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद कर रहे हैं तो आपकी अंग्रेज़ी भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, यह पहली शर्त है और दूसरी शर्त यह है कि आपको दोंनो भाषाओं के साथ-साथ विषय का भी ज्ञान होना चाहिए । अगर आप इतिहास का काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा इतिहासकार होना चाहिए। अगर आप अर्थशास्त्र या दर्शनशास्त्र नहीं जानते हैं और आपको इन विषयों का ज्ञान नहीं है तो आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। और तीसरी शर्त यह है कि आपको सृजनात्मक होना चाहिए, खास तौर पर अगर आप ललित साहित्य का अनुवाद करना चाहते हैं तो आपको स्वयं एक अच्छा लेखक, कवि या रचनाकार होना चाहिए क्योंकि उसमें जो सृजनात्मकता का गुण है, उसकी जो अनुभूति है, जब तक आप स्वयं उसका अनुभव नहीं करेंगे आप अच्छा अनुवाद नहीं कर सकते। शाब्दिक अनुवाद जो मक्खी पर मक्खी मारने वाली बात है, वह अनुवाद नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि साहित्यिक अनुवाद मौलिक लेखन से भी कठिन काम है, कठिन काम है! जैसे मैंने ‘युद्ध और शांति' का अनुवाद किया, इस पुस्तक के 1500 पृष्ठ हैं और इसमें कई सौ पात्र हैं, कई सौ! कैसी-कैसी कठिन परिस्थितियाँ हैं इसमें, कि कैसे नेपोलियन आया फ्रांस से रूस को विजय करने के लिए और कैसी-कैसी परेशानियाँ झेलीं उन लोगों ने। कैसे लड़ाइयाँ हुईं, युद्ध के दृश्य! मैं कभी सैनिक नहीं रहा तो उन दृश्यों को समझना, उनकी गहराइयों में जाना और फिर उन्हें अपनी भाषा देना - मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन काम है। जिसका आप अनुवाद कर रहे हैं उसे आपको जीना चाहिए उसी रूप में तभी बात बनती है और पाठक को लगता है कि वह अपनी भाषा की कोई मौलिक रचना पढ़ रहा है। 'युद्ध और शान्ति' का अनुवाद करने में मुझे साढ़े चार - पाँच साल लग गए । राजकमल वालों ने 'आना करेनिना ' के पिछले सालों में कई-कई संस्मरण निकाल दिए क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि लीव तॉल्स्तॉय को अंग्रेज़ी में पढ़कर मज़ा नहीं आता था अब हिंदी में पढ़कर अपना-अपना सा लगता है।
युवा भारतीय हिंदी पढ़ना नहीं चाहते, हिंदी का महत्व कम होता जा रहा है। हिंदी में अंग्रेज़ी शब्दों के बढ़ते चलन से हिंदी भाषा का स्वरूप ही बिगड़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है, क्या कमी रह गई और भविष्य में इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अंग्रेज़ 200 साल तक भारतीयों को यह घुट्टी पिला गए। हालाँकि अंग्रेज़ी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इसका अच्छा ज्ञान होना भी ज़रूरी है और लाभदायक भी, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी भाषा की तरफ ध्यान न दें। इसमें कोई बुराई नहीं है कि कहीं-कहीं दूसरी भाषा के शब्द बीच-बीच में आ जाएं बोलचाल में लेकिन हिंदी की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। युवा पीढ़ी को खासकर चाहिए कि वे अपनी भाषा को सीखें, उसे पढ़ें और जहाँ तक सम्भव हो उसे बनाए रखें। इसके लिए यत्न करने की ज़रूरत है, हमारे कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हिंदी के स्वरूप और महत्व को बनाए रखें । कम से कम दसवीं-बारहवीं तक तो हिंदी अच्छी आनी चाहिए, अच्छी हिंदी। इसके लिए शिक्षकों को, प्रोफेसरों को, टीचरों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को इस ओर प्रेरित करें। शिक्षा संस्थानों को, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ।
-सुनीता पाहूजा
सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो